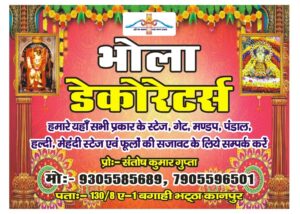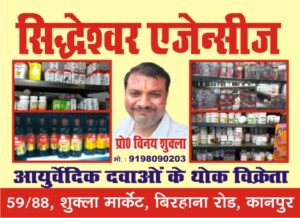पंकज कुमार मिश्रा, मिडिया विश्लेषक एवं पत्रकार जौनपुर यूपी
एक दिन में ही जाति व्यवस्था समाप्त किया जा सकता है किन्तु इसका परिणाम सोचिये ! संकल्पनायें सोचिये, भविष्य सोचिये और फिर सामाजिक व्यवस्था का संचालन कैसे होगा यह सोचिये। किसी भी व्यक्ति का समाज में उसके कर्म की पहचान का एकमात्र सूचक उसकी जाति है। यह सूचित करता है की उसको किस व्यवस्था में समाज में योगदान देना है। इसी के आधार पर कोई किसी को अपना समझाता है या एजेंडे में फंसकर विद्वेष करता है। यदि वह व्यक्ति बीमार मानसिकता का है तो वह अपने जाति के लोगो को पुरानी सनातन व्यवस्था के खिलाफ भड़कायेगा और यदि किसी व्यक्ति को कभी अपना नाम, या उपनाम रखने, संशोधित करने, एवं बदलने का अधिकार एवं सुविधा दे दिया जाय तो वह इसका उपयोग निजी स्वार्थ हेतु करेगा। क्या इससे कोई अराजकता नहीं आएगी.? किसी व्यक्ति का आधार संख्या निर्धारित एवं निश्चित होता है, शासन को यह व्यवस्था करना चाहिए की आधार संख्या के आधार पर एक ऐसा डाटा बैंक तैयार करें जिसमें उसकी वर्तमान स्थिति नौकरी और आय लिखी हो ताकि उसके समाज के अन्य लोग उस व्यक्ति को मिलने वाले आरक्षण के सहारे आगे आ सके ,जो मूल आरक्षित वर्ग के पहचान को संरक्षित एवं सुरक्षित रखेंहुए है। इस आरक्षित एवं मूल आंकड़े को देखने का अधिकार किसी जिलाके वरीय पुलिस अधिकारी को होगा, जो किसी अपराध के अन्वेषण में इसे आवश्यक समझता है। इसके साथ ही ऐसा अधिकार किसी नियोक्ता एजेंसी को भी होगा, जो आरक्षण का लाभ देता है। इन आकड़ों को देखे जाने का कारण उस तंत्र के प्रणाली में दर्ज करना होगा, और यह देखे जाने की प्रविष्टि भी स्थायी रूप से अंकित रहेगी। इसके अतिरिक्त इसकी सत्यता किसी को ज्ञात नहीं होगा और अयोग्य आरक्षण कोटा वाले योग्य और अनारक्षित होते रहेंगे । इस तरह नई जाति एवं नव बौद्ध जैसे सूचक शब्द बेकार एवं असंगत हो जायेंगे। धीरे- धीरे यह प्रचलन से ही बाहर हो जायेंगे।
वर्तमान में जिस समाज में हम जी रहे हैं और जो समाज है अपने वंशजों के लिए छोड़कर जाने वाले हैं उसकी स्थिति धर्म की दृष्टि में अत्यंत भयावह है। सर्वत्र अनेकानेक पंथ अपने आपको सत्य पुरातन बताने में लगे हुवे हैं। हर मत स्वयं को सच्चा और दुसरे को झूठा बता रहा है और इसके लिए आस सम्पूर्ण विश्व सनातन धर्म के नाश की कामना कर रहा है।ऐसी विषम परिस्थिति में वर्ण व्यवस्था, जिसे सनातन धर्म का मेरुदंड कहते हैं, की रक्षा एक चुनौती भरा कार्य है| भारत में प्रबल रूप से वर्ण व्यवस्था व ब्राह्मणों का विरोध चल रहा है। इस अंध विरोध का जो कारण मुझे समझ में आता है वो है वर्ण व्यवस्था को सही तरीके से न समझा पाना। आजकल लोग ये कह देते हैं कि शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है आदि आदि, और फिर इसके कारण प्रमाद फ़ैल जाता है। वर्तमान का मनुष्य इतना समझदार नहीं है की वो इन बातों की गूढ़ता को समझ सके तो हमें ही अपनी भाषा बदल देनी चाहिए। इसी बात को हम इस प्रकार से कह सकते हैं की शूद्रों से भदवद्प्राप्ति का सबसे सुगम मार्ग प्रदान है और ब्राह्मणों को सबसे दुष्कर। ब्राह्मण पर तो सबसे अधिक निषेध हैं, जितने कड़े नियमों व अनुशासन का पालन ब्राह्मण को करना चाहिए उतना तो किसी के लिए नहीं है। ब्राह्मणों में भी सबसे अधिक निषेध शंकराचार्य पर हैं। वे तो अग्नि प्रज्ज्वलन भी नहीं कर सकते। जब हम कहते हैं की आपको इसका अधिकार नहीं है तो उसे लगता है की उसे वंचित रखा गया है पर नहीं उसे वंचित नहीं रखा गया है बस उसके लिए मार्ग अलग है। सनातन धर्म में फल से तो किसी को वंचित रखा ही नहीं गया। जिस मोक्ष का अधिकार एक शंकराचार्य रखते हैं उसी मोक्ष का अधिकार एक शूद्र भी रखता है। अंतर है तो दोनों के मार्ग का। शंकराचार्य जी को न जाने कितने नियम व अनुशासन का पालन करना पड़ेगा और वहीँ एक शूद्र केवल भगवान का नाम जप के मोक्ष प्राप्त कर लेगा। कुछ लोग बोलते हैं की वर्ण व्यवस्था ने लोगों को बाँट दिया। तो पहले तो हम यह समझ लें की वर्ण व्यवस्था विभाजन नहीं वर्गीकरण करती है और ये वर्गीकरण जन्मजात गुणों के आधार पर है। इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं की संसार की चार अभीष्ट अभिलाषाएं हैं – सम्मान, यश, धन, निश्चिंतता| हर मनुष्य इन चारों की अभिलाषा रखता है परन्तु बहुलता किसी एक की ही प्राप्त क्र पाता है। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके पास सर्वोच्च सम्मान, सर्वोच्च यश, सर्वाधिक धन और पूर्ण निश्चिंतता हो। सनातन धर्म में इन चारों को चारों वर्णों में बाँट दिया गया है। ब्राह्मणों को सम्मान प्राप्त है, क्षत्रिय को यश प्राप्त है, वैश्य को धन प्राप्त है और शूद्रों को निश्चिंतता प्राप्त है। ब्राह्मण को सम्मान अवश्य प्राप्त है परन्तु ब्राह्मण का यश नहीं होता, वह धनी भी नहीं होता और निश्चिंतता का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता क्योंकि विश्व के कल्याण का दायित्व ब्राह्मण का ही है। शूद्र को सम्मान याश या धन तो नहीं दिया पर निश्चिंतता दे दी। निश्चिंतता वो वरदान है जो आज किसी के पास नहीं और इसे प्राप्त वही कर सकता है जो सम्मान यश और धन का त्याग कर देगा क्योंकि ये तीनों ही चिंता के कारक हैं। अब देखिये कर्मों का विभाजन कैसे हुव। ब्राह्मण को मिला पौरोहित्य, तपश्चर्य, अध्ययन, अध्यापन आदि का कार्य, क्षत्रिय को मिला राजनीति, रक्षा, प्रजापालन का दायित्व, वैश्य को कृषि, गौरक्षा और वाणिज्य प्राप्त हुवा और शूद्र को कुटीर व लघु उद्योग और सेवा के समस्त प्रकल्प प्रदान हुवे। अब प्रश्न उठ सकता है कि कर्म के विभाजन की आवश्यकता क्या है? जिसकी जो इच्छा हो वह कर्म करे। पहली बात इच्छानुसार कर्म केवल अराजकता को ही जन्म देगा और वर्तमान में यह बात चरितार्थ भी हो रही है। इच्छानुसार कर्म की स्वतंत्रता ने बेरोजगारी जैसी समस्या को उत्पन्न कर दिया| यदि हम ध्यान दें तो देखेंगे की किसी एक कार्यालय को चलाने के लिए कार्यों का विभाजन और अधिकारों की सीमा तय की जाती है। अब आप खुद सोचिये की जब एक कार्यालय बिना कार्य विभाजन के नहीं क्रियान्वित हो पता तो समाज का क्रियान्वयन इच्छानुसार कर्म और बिना कर्म के विभाजन के कैसे होगा? दूसरी बात यह कर्म का विभाजन आतंरिक जन्मजात गुणों के आधार पर हुवा है। यदि हम जेम्स डी वाट्सन की जींस थ्योरी पढ़ें तो हमें ज्ञात होगा कि हर जन समूह के जींस की संरचना भिन्न होती है और इस कारन उनके गुण भी भिन्न होते हैं| इसी बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक ब्राह्मण की रुचि स्वाभाविक रूप से किसी ज्ञान के ही क्षेत्र में होती है, एक क्षत्रिय की रुचि वीरता, राजनीति व प्रभुत्व स्थापित करने में जन्म से ही होती है, एक वैश्य की रुचि जन्म से ही व्यापार में होती है और इसी प्रकार एक शूद्र की रुचि कुटीर उद्योग अथवा सेवा के प्रकल्पों में ही होती है। अब ये तो जबरदस्ती की बात है कि सभी एक हैं इसलिए सबको कलक्टर बना दो पर आप आज भी किसी के आतंरिक गुणों की उपेक्षा नहीं कर सकते। अब थोड़ी बात समानता पर भी कर लेते हैं। आज लोग समानता का दृष्टिकोण जड़ को लेकर करने लगे हैं और चेतन को छोड़ देते हैं पहले तो हम यह समझ लें कि हम क्या हैं ? हम यह शरीर हैं या इस शरीर से भिन्न कुछ और हैं ? मान लीजिये कि आपकी ऊँगली कट जाए तो आप क्या कहेंगे ? मरे ऊँगली कट गई या मैं कट गया ? निस्संदेह आप कहेंगे कि मेरी ऊँगली कट गई अर्थात यह “मैं” इस शरीर से भिन्न कुछ और है अर्थात आत्मा। अतः हम शरीर नहीं आत्मा हैं। जब हम यह जान लेंगे कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं तो हम समानता की बात आत्मा को ध्यान में रखकर करेंगे न कि शरीर को। अब आत्मा क्या है ? पहले तो यह जान लेना आवश्यक है कि आत्मा नित्य है और अवध्य है अर्थात आत्मा सदा थी सदा रहेगी। प्रलय के बाद फिर सृष्टि होगी परन्तु आत्मा यही रहेगी। अब यह आत्मा है क्या? तुलसीदास जी लिखते हैं कि “ईश्वर अंस जीव अविनासी” अर्थात जीव (आत्मा) ईश्वर का अंश है। अब इसका क्या अर्थ हुआ ? यही कि जिन ८४ लाख योनियों की सृष्टि भगवान ने की उन सभी में वद्यमान जीव ईश्वर का ही अंश है और इस प्रकार न कोई छोटा है न कोई बड़ा।